Shekhar Gupta’s column – We can bring about major agricultural reforms by turning Trump’s tariff policy to our advantage | शेखर गुप्ता का कॉलम: हम ट्रम्प की टैरिफ नीति को अपने फायदे में बदलकर बड़े कृषि-सुधार कर सकते हैं
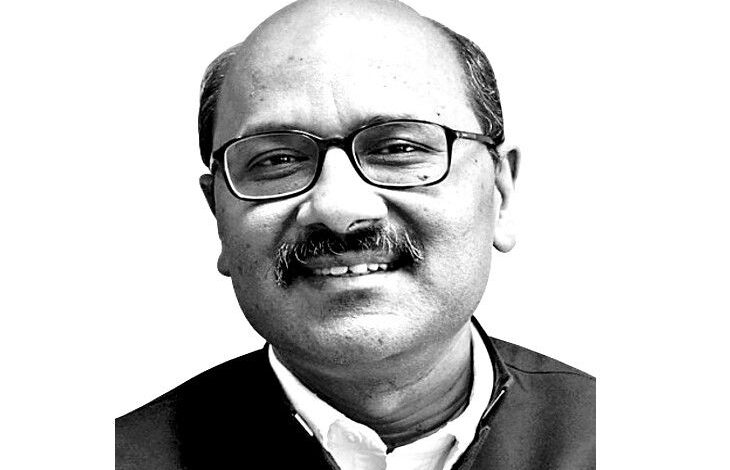
- Hindi News
- Opinion
- Shekhar Gupta’s Column We Can Bring About Major Agricultural Reforms By Turning Trump’s Tariff Policy To Our Advantage
2 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
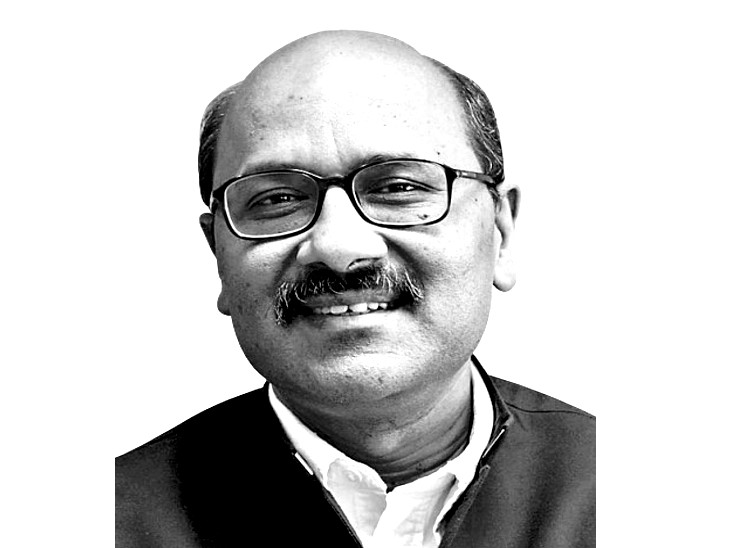
शेखर गुप्ता, एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’
एमएस स्वामीनाथन जन्म-शताब्दी कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि किसानों, मछुआरों और डेयरी से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा वे हर हाल में करेंगे- चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े। यह कीमत कौन-सी है?
भारत के लोग अपनी सम्प्रभुता को सबसे ऊपर रखते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए वे अस्थायी नौकरियों के नुकसान को भी चुपचाप सह लेते हैं। झींगा पालन करने वाले किसान, बासमती और मसाले उगाने वाले, कालीन बुनकर, होजयरी कामगार और गुजरात के हीरे-रत्न काटने-जोड़ने और सोने के आभूषण बनाने वाले कारीगर- इन सभी पर 50% टैरिफ का असर पड़ेगा।
एक और वर्ग है, जो शायद इन सबके बराबर संख्या में है- किसान। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर बासमती चावल, मसाले, फल-सब्जियां, पैकेज्ड फूड, चाय-कॉफी निर्यात करता है, जिसकी कुल कीमत 6 अरब डॉलर से अधिक है। 50% टैरिफ लगने पर यह सब टिक पाना मुश्किल होगा।
लेकिन अमेरिका को चुनौती देना भारत के किसी नेता के लिए निजी जोखिम नहीं होता। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा आत्मविश्वास के साथ किया था और उन्हें इसका फायदा मिला था। विदेशी दबाव की बात आते ही भारत आमतौर पर अपने मौजूदा नेता के पीछे एकजुट हो जाता है।
इस मायने में, मोदी के लिए कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त वे बेहद दृढ़ दिख रहे हैं, हम उन्हें एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा कर सकते हैं, जिसमें वास्तव में जोखिम हो सकते हैं। अगर यह सफल हुआ, तो यह कृषि में क्रांति ला सकता है। इससे न केवल अगले पांच साल में किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकेगी, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
जिस मौके पर मोदी बोल रहे थे, वह मायने रखता है। स्वामीनाथन- जिन्हें इस सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया- को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और उन्हें भारत को जहाज से अनाज मंगाने वाली शर्मिंदगी से मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है।
1960 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की सरकार को बस अगला अनाज का जहाज रोकना होता था और भारत परेशान हो जाता था। उस समय उनकी शर्तों में से एक यह भी थी कि भारत जनसंख्या वृद्धि पर सख्ती से लगाम लगाए। वह दौर हरित क्रांति और 1971-72 तक अनाज में आत्मनिर्भरता के साथ खत्म हुआ।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्वामीनाथन और उनके साथियों- जिनमें महान अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग भी शामिल थे- के तरीकों को लेकर उस समय कड़ी आलोचना भी हुई। सबसे ज्यादा विरोध करने वालों में एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट थे।
उस दौर में हाइब्रिड बीजों को लेकर बहुत डर था और यह शंका भी कि कोई भी मशीनीकरण सिर्फ बड़े किसानों के फायदे का होगा। इसी वजह से स्वामीनाथन के नेतृत्व में सुधारकों के समूह ने पहले खेत परीक्षण छोटे किसानों के साथ शुरू किए।
1966 में इंदिरा सरकार के लिए 18,000 टन हाइब्रिड बीज (मूल्य 5 करोड़ रु.) प्रदर्शन के लिए मंगाने की अनुमति देना कितना मुश्किल था, पर इंदिरा ने हिम्मत दिखाई। जोखिम यह था कि नए बीज कोई खतरनाक रोग ला सकते थे, या प्रयोग पूरी तरह असफल हो सकता था, लेकिन इंदिरा ने जोखिम लिया और इनाम मिला, भारत को भूख और अपमान से मुक्ति।
जंग के समय जोखिम उठाना मजबूरी है, लेकिन सबसे साहसी नेता वे होते हैं जो शांति के समय भी जोखिम चुनते हैं। इसके लिए एक ठोस कारण, एक धक्का चाहिए। 1991 में, नरसिंह राव-मनमोहन सिंह के लिए यह कारण था भुगतान संकट।
1999 में, वाजपेयी के लिए यह कारण बना पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगे प्रतिबंध। पिछले 20 साल में हमें वैसा कोई बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ा और पिछले 25 साल की तेज विकास दर ने हमें लापरवाह भी बना दिया है।
जानकार और विशेषज्ञ लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा, व्यापार की शर्तें, टैरिफ घटाने जैसे कई जरूरी सुधारों की बात कर रहे हैं। हर सुधार कठिन है, खासकर हमारे प्रशासनिक ढांचे में। लेकिन जैसे पहले संकटों ने भारत में उद्योग, वित्त, प्रतिस्पर्धा और तकनीक में बड़े सुधार लाए, वैसे ही क्यों न इस मौके का इस्तेमाल कृषि सुधारों के लिए किया जाए?
सच कहें तो हरित क्रांति के बाद से भारतीय कृषि दूसरे गियर में ही चल रही है। आखिरी बड़ा कृषि सुधार वाजपेयी सरकार ने 2002 में किया था, जब उन्होंने जीएम कपास के बीज को मंजूरी दी- जबकि उनके स्वदेशी समर्थकों का जोरदार विरोध था। पोखरण-2 के बाद वे पहले ही जय जवान, जय किसान को जय विज्ञान तक बढ़ा चुके थे।
2002-03 से 2013-14 के बीच, कपास का उत्पादन 1.36 करोड़ गांठ से बढ़कर 3.98 करोड़ गांठ हो गया- यानी 193% की छलांग। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 302 किलो से बढ़कर 566 किलो हो गया। भारत, जो हमेशा कपास आयात करता था, बड़ा निर्यातक बन गया और 2011-12 में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात किया। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। सबसे ज्यादा फायदा गुजरात के किसान को हुआ, जिन्हें इस दशक में 8% की औसत वृद्धि मिली। लेकिन आज भारत फिर से कपास आयात कर रहा है।
भारत को सोयाबीन और मक्का (कॉर्न) चाहिए- वही दो फसलें जिन्हें अमेरिका हमें बेचना चाहता है। हमें इनकी कमी क्यों है? सबसे बड़ा कारण है विज्ञान का डर। आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन फिर भी लगभग 24 अरब डॉलर का खाद्य तेल और दालें आयात करते हैं।
इसके अलावा लगभग 10 अरब डॉलर के उर्वरक भी आयात करते हैं। हम 332 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं और चीन 706 मिलियन टन पैदा करता है। खेती जीडीपी में लगभग 16% योगदान देती है, लेकिन हमारे 50% से ज्यादा मतदाता इससे जुड़े हैं। ट्रम्प की टैरिफ नीति भारत के लिए एक नई हरित क्रांति लाने का मौका है।
राजनीतिक नेतृत्व को हिम्मत दिखानी होगी… आज जीएम बीजों का डर वही है, जो 1960 के दशक में हाइब्रिड बीजों के लिए था। राजनीतिक नेतृत्व को आज वही हिम्मत दिखानी होगी, जैसी इंदिरा गांधी ने 1966 में दिखाई थी। ध्यान रहे कि आज 78 देश लगभग 220 मिलियन हेक्टेयर में जीएम बीज उगा रहे हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)
Source link


