Shekhar Gupta’s column – We can learn important lessons from Europe | शेखर गुप्ता का कॉलम: यूरोप से जरूरी सबक सीख सकते हैं हम
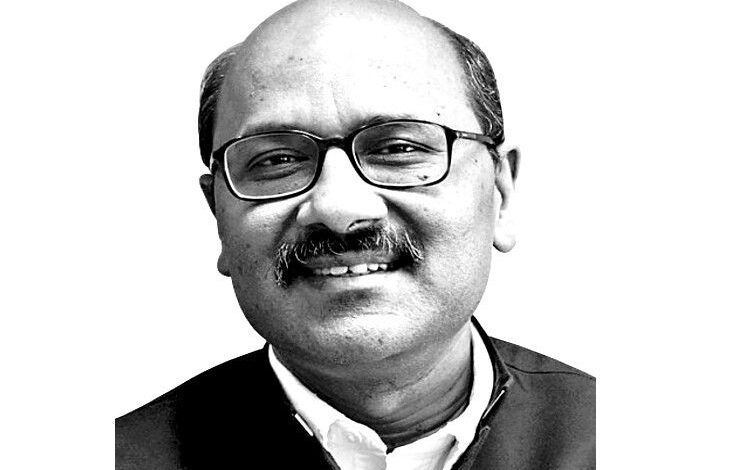
3 घंटे पहले
- कॉपी लिंक

शेखर गुप्ता, एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिन्ट’
एक पल के लिए उस तस्वीर पर गौर कीजिए, जिसे कई पीढ़ियों तक याद किया जाता रहेगा : जेलेंस्की समेत यूरोपीय संघ के बड़े नेता ‘शाही हेडमास्टर’ ट्रम्प के सामने माफी मांगते हुए स्कूली बच्चों की तरह बैठे हैं! उसे देखकर सबसे पहले आपके अंदर कौन-सी भावना उभरती है?
सहानुभूति की या मनोरंजन की या दया की या नई उभरती विश्व-व्यवस्था के एहसास की? वैसे, पूरी संभावना यह है कि सहानुभूति को छोड़ इस सबका मिला-जुला एहसास ही मन में उभरेगा और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ट्रम्प के सताए हुए हैं।
हम देख सकते हैं कि कम-से-कम एक नेता तो ऐसा है, जिसके मन में इस तरह का कोई भावनात्मक घालमेल नहीं है। पुतिन इस सबको खालिस हिकारत की नजर से देखते हैं। जबकि दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश; सबसे बड़ी तीसरी और छठी अर्थव्यवस्थाएं, दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक खेमा (ईयू); परमाणु हथियारों से लैस दो पी5 देश, सबके सब घुटने टेके नजर आए।
वे सब ट्रम्प के दरबारी बने नजर आए, जबकि पुतिन इस खेमे को कमजोर करने में लगे हैं। पुतिन इसे इस बात की स्वीकृति के रूप में देखते हैं कि युद्ध उन्होंने जीता है। जीत को परिभाषित करना उन पर निर्भर है। यूरोपीय लोग इसे उलटे रूप में देखते हैं, जिन्हें अब इसे एक बुरी हार के रूप में देखने की जरूरत नहीं।
पुतिन को अब पता चल गया है कि उन्होंने 2022 में जो आक्रमण शुरू किया था, सिर्फ उसमें कब्जाए गए इलाके ही नहीं, बल्कि क्रीमिया और डोनबास भी उनके अपने हैं। यह यूक्रेन के विशाल भूभाग के करीब 20 फीसदी के बराबर है। इसके अलावा, पूरब की ओर ‘नाटो’ का विस्तार अब इतिहास की बात हो गई है।
ट्रम्प यह अकसर कह चुके हैं। हमें यह तो मालूम है कि वे अपना दिमाग बदलते रहते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम ही है कि वे अचानक यूक्रेन और यूरोप की सपनीली मांगों का समर्थन करने लगेंगे, जिनमें पुतिन की हार शामिल है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे क्या रियायत कर सकते हैं। पुतिन उसे कबूल करके और ज्यादा के लिए वार्ता कर सकते हैं।
रूस को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने हमला जारी रखा है, चाहे प्रगति कितनी ही धीमी और खर्चीली क्यों न हो। अगर इस मुकाम पर शांति कायम होती है तो पुतिन अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं। वे अपनी विजय घोषणा क्रीमिया या मारीउपोल से कर सकते हैं।
शांति बहाल होने के बाद आर्थिक प्रतिबंध भी हट जाएंगे। तब वे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने में लग जाएंगे। उनका वजन इस बात से बढ़ा है कि उन्होंने ट्रम्प को यह विश्वास दिला दिया है कि वे लड़ना जारी रख सकते हैं, चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े।
यूक्रेन को अर्ध-सम्प्रभु देश में बदलने की पुतिन की बड़ी मांग- जिसमें सरकार उनकी पसंद की हो- अगर खारिज कर दी गई है तो इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने अविश्वसनीय बहादुरी और चुस्ती से लड़ाई लड़ी। पश्चिमी मित्र देशों और अमेरिका ने संसाधनों से बेशक उसकी मदद की, लेकिन यूक्रेनियों ने एक सम्प्रभु देश के रूप में अपना वजूद इतनी लंबी लड़ाई लड़ कर और पुतिन के रूस जैसे कठोर देश से उतनी कीमत वसूल करके बचाया है, जिसे वही बर्दाश्त कर सकता था।
उन्होंने दुनिया को ड्रोन के बूते दूर जाकर ऐसे पैमाने पर युद्ध लड़ना भी सिखाया है, जिससे मोसाद को भी ईर्ष्या हो सकती है। मात्र 3.5 करोड़ की छोटी-सी आबादी के (जिसका करीब 20 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह रहा है) अनुपात से हताहतों की भारी संख्या को उसने बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया है।
उन्होंने रूसियों को कहीं बड़ी संख्या में अपने सैनिक गंवाने पर मजबूर किया है और उनकी अर्थव्यवस्था तथा सैन्य तंत्र को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन को दो वजहों से बेहतर नतीजे नहीं हासिल हुए। पहली यह कि उसके यूरोपीय सहयोगी सैन्य या आर्थिक मोर्चे पर कोई नुकसान सहने को राजी नहीं हुए और दूसरी यह कि ट्रम्प सत्ता में वापस आ गए।
इतना स्पष्ट करने के बाद हम ट्रम्प के ओवल ऑफिस की उस ऐतिहासिक तस्वीर की ओर लौटते हैं। यूरोप ने खुद को एक विशाल गुलाम-क्षेत्र में कैसे तब्दील कर लिया, इस पर कई किताबें लिखी जाएंगी। यूरोप अपनी राजी-खुशी से ट्रम्प के नव-साम्राज्यवाद का पहला शिकार बना, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरोप भावना में बहकर नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है।
इसलिए भारत के लिए सबक ये हैं कि अपनी सेना को मजबूत बनाइए और इसके लिए उपयुक्त उपमा यही होगी कि यह युद्धस्तर पर कीजिए। अभी से शुरुआत की जानी चाहिए। रूस के साथ रिश्ता और मजबूत कीजिए, लेकिन किसी खेमेबंदी में पड़ने से बचिए।
लोकतांत्रिक भारत का भविष्य पश्चिम-विरोध में नहीं है। चीन के मामले में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है उसमें स्थिरता बनाए रखिए और दोनों पक्षों को उस दिशा में बढ़ने दीजिए जिससे उनके साझा हित पूरे होते हों। याद रहे, चीन को अभी हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपना ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित कीजिए।
अपने पड़ोस को शांत रखिए। भारत को सभी मोर्चों पर दुश्मनी में नहीं उलझना चाहिए। पाकिस्तान का मामला अलग है, लेकिन हर एक पड़ोसी के साथ रिश्ते में घरेलू राजनीति की घालमेल करने से बचिए। इससे आपके विकल्प सीमित होते हैं। अपना वक्त चुनिए और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते में कुछ समझदारी लाने की कोशिश कीजिए।
भरोसा पैदा करना मुश्किल हो सकता है। याद रहे, शीतयुद्ध वापस नहीं आने वाला और अमेरिका/पश्चिम विरोधी खेमा उभरने वाला नहीं है। यूक्रेन में अमन कायम होते ही पुतिन और ट्रम्प फिर दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और चीन तो सौदे करने में व्यस्त हो ही गए हैं। यूरोप से सीखिए। ट्रम्प के कारण जो अफरा-तफरी मची है वह व्यवहार-कुशलता के बूते ही दूर की जा सकेगी।
खेमेबाजी से बचें, पश्चिम- विरोध का भविष्य नहीं है… यूरोप भावना में बहकर नहीं बल्कि हकीकत के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है। भारत के लिए सबक ये हैं कि सेना को मजबूत बनाइए। रूस से रिश्ता मजबूत कीजिए, लेकिन किसी खेमेबंदी में पड़ने से बचिए। लोकतांत्रिक भारत का भविष्य पश्चिम-विरोध में नहीं है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)
Source link


