Prof. Ram Singh’s column- Is there more equality in the country than before? | प्रो. राम सिंह का कॉलम: क्या देश में पहले की तुलना में अधिक समानता आई है?
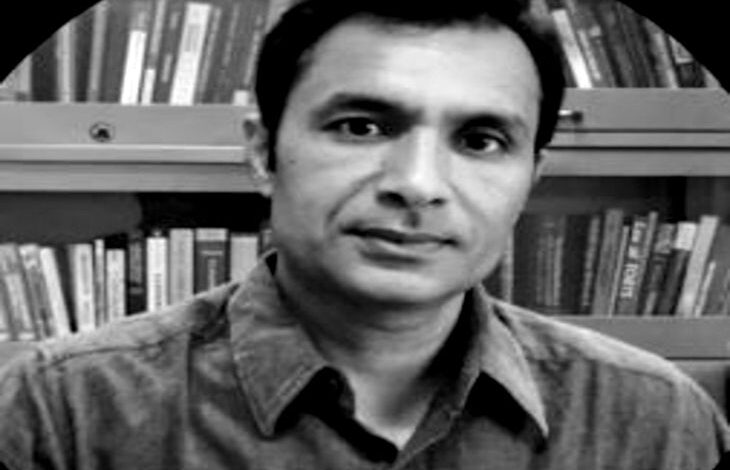
- Hindi News
- Opinion
- Prof. Ram Singh’s Column Is There More Equality In The Country Than Before?
4 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
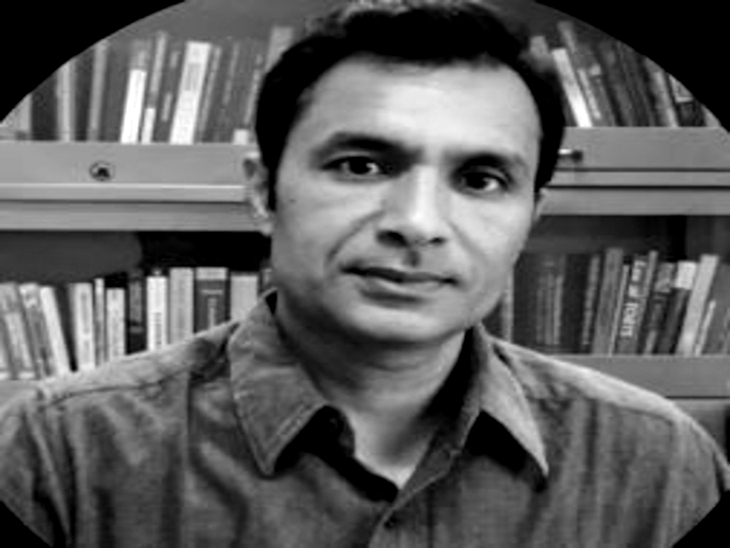
प्रो. राम सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर
विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत ने उपभोग की असमानता को काफी हद तक कम किया है। अर्थशास्त्री गरीब और अमीर के बीच असमानता को मापने के लिए गिनी इंडेक्स का उपयोग करते हैं। गिनी वैल्यू में कमी को अच्छा माना जाता है।
विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत का गिनी इंडेक्स घटा है। इस मानदंड पर भारत दुनिया के चार सबसे समानता वाले देशों में शुमार हो गया है। भारत की स्थिति चीन, अमेरिका और यूके से कहीं बेहतर बताई गई है।
यहां गौर करना होगा कि भारत के लिए विश्व बैंक के आकलन उपभोग की असमानता के संदर्भ में हैं। इसके लिए उसने विभिन्न समूहों के उपभोग खर्च पर कराए गए एचसीईएस 2022-23 के आधिकारिक डेटा का उपयोग किया है। इसमें उसने सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त सामानों में से कुछ वस्तुओं के उपभोग खर्च के मूल्य को भी जोड़ा है।
देश में बड़े पैमाने पर व्याप्त विषमताओं संबंधी मीडिया रिपोर्टों के अभ्यस्त हो चुके कई लोगों ने भारत में घटी उपभोग असमानता के दावे पर या तो संदेह जताया है या इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आलोचकों का तर्क है कि एचसीईएस के उपभोग डेटा में अमीरों के उपभोग को सटीकता से शामिल नहीं किया गया है।
उनके अनुसार उपभोग की असमानता विश्व बैंक के आकलन से अधिक है। वे पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब (डब्लयूआईएल) की रिपोर्ट के आधार पर भी कहते हैं कि भारत में आय की असमानता बहुत अधिक है। ऐसे में स्वस्थ बहस के लिए हमें इस विवरण में छिपी चीजों को खंगालना होगा।
हम विश्व बैंक के आकलनों पर चाहे जितनी बहस करें, लेकिन एनएसएसओ के डेटा से स्पष्ट है कि भारत में उपभोग की विषमता में आई कमी उल्लेखनीय है। भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग भी सुधरी है। विश्लेषक राष्ट्रीय आय में शीर्ष 1% वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर चिंता जता रहे हैं।
ये उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूआईएल के अनुमानों में कई खामियां हैं, जिससे अतिशयोक्तिपूर्ण दावे पैदा होते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आय के वितरण को लेकर भारत में आज भी कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। डल्ब्यूआईएल ने शीर्ष आय वर्गों के अनुमान के लिए आयकर के डेटा का प्रयोग किया है।
निम्न और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए उसने माना है कि इनमें से 70 से 80% परिवारों का उपभोग खर्च उनकी आय से अधिक होता है। सरल शब्दों में आय की असमानता के अनुमान कहते हैं कि शीर्ष 20 से 25% परिवारों के अलावा शेष सभी साल-दर-साल अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं।
इस अव्यावहारिक धारणा के चलते निचले 80% वर्ग की आय को कम करके आंका गया है। इससे राष्ट्रीय आय में इस वर्ग की हिस्सेदारी उनकी वास्तविक हिस्सेदारी से कम आंकी गई है। जबकि शीर्ष आय समूहों की हिस्सेदारी का अनुमान वास्तविकता से अधिक है।
क्या देश आय की असमानता बढ़ रही है? जवाब है, नहीं। यदि हम डब्ल्यूआईएल के दावों को भी देखें तो 2017 से 2022 के बीच राष्ट्रीय आय में निचले 50% वर्ग का हिस्सा बढ़ा है, जबकि शीर्ष 10% का घटा है। शीर्ष 1% वर्ग की अधिक हिस्सेदारी यकीनन चिंता का विषय है।
हालांकि, 2016-17 से इस 1% वर्ग का हिस्सा केवल 0.3% ही बढ़ा है। यह केंद्र सरकार द्वारा कर चोरी रोकने के उपायों के चलते हुआ है। पहले की तुलना में उच्च आय वर्ग आजकल सत्यतापूर्ण रिपोर्ट देते हैं। मेरा शोध कहता है कि 2014 से शीर्ष आय वर्ग की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी कर संबंधी नियमों के बेहतर अनुपालन के कारण हुई है। इसे बढ़ती असमानता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।
वास्तव में आय की असमानता का आकलन लोगों की क्रयशक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कर-पूर्व आय के स्थान पर कर चुकाने के बाद बची आय के आधार पर। चूंकि अमीरों द्वारा करों का भुगतान बढ़ा है, इसलिए शीर्ष आय वर्ग की कर-पश्चात आय उनकी कर-पूर्व आय का सिर्फ 65 से 70% हिस्सा ही रह गई है, जिसके आधार पर आय की समानता का आकलन किया गया है।
इसके विपरीत, निम्न आय समूहों के लिए असमानता अनुमानों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत कैश ट्रांसफर को शामिल नहीं किया जाता। जबकि आज इस तरह के ट्रांसफर जीडीपी का लगभग 8% हैं। यदि हम अमीरों की कर देने की बाद की आय का उपयोग करें और गरीबों की आय में सब्सिडी जोड़ें, तो पाएंगे कि बीते एक दशक में आय असमानता में कमी आई है।
हम विश्व बैंक के आकलनों पर चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन यह भी याद रखें कि भारत में उपभोग की विषमता में आई कमी उल्लेखनीय और निर्विवाद है। इसी प्रकार भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में आया सुधार भी तथ्यपूर्ण है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
Source link



